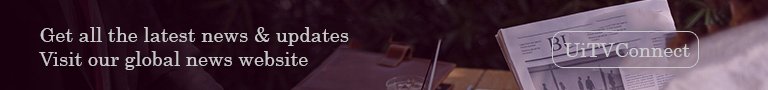नई दिल्ली,24 सितंबर (युआईटीवी)- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) में शामिल बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) अध्याय को लेकर एक उच्चस्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नीति निर्माताओं,शिक्षाविदों,डोमेन एक्सपर्ट्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस अध्याय से जुड़े अवसरों एवं चुनौतियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
यह सेमिनार वाणिज्य भवन में आयोजित किया गया था,जिसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ (सीटीआईएल) के सहयोग से आयोजित किया। इसका विषय था—“भारत-यूके सीईटीए में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) अध्याय का रहस्य उजागर।” विशेषज्ञों ने इसे समय की माँग बताते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और नवाचार के बीच भारत को अपनी भूमिका मजबूत करनी होगी और आईपीआर इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है।
सेमिनार में उपस्थित विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि बौद्धिक संपदा अधिकार अध्याय का उद्देश्य नवाचार और पहुँच के बीच संतुलन स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर यह अध्याय भारत के आईपी फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाएगा,वहीं दूसरी ओर यह जन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों ने आश्वस्त किया कि इन प्रावधानों के जरिए स्वास्थ्य,शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जनता की पहुँच प्रभावित नहीं होगी।
इस चर्चा में एक प्रमुख मुद्दा पेटेंट प्रक्रियाओं के सामंजस्य का था। कुछ वर्गों में यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इन प्रक्रियाओं से भारत की नियामक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। हालाँकि,विशेषज्ञों ने इस भ्रांति को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि यह केवल प्रक्रियात्मक सुधार हैं और किसी भी रूप में भारत की नीति बनाने की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करते। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है और यह समझौता उसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर कहा कि सीईटीए का आईपीआर अध्याय भारत के स्टार्टअप्स,एमएसएमई और पारंपरिक उत्पादकों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे उद्योगों को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। वहीं पारंपरिक उत्पादक अपने क्षेत्रीय और सांस्कृतिक उत्पादों को मजबूत कानूनी संरक्षण दिला सकेंगे,जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान और मूल्यवर्धन का लाभ होगा।
सेमिनार में भारत-ब्रिटेन व्यापार वार्ता के दौरान भारतीय भौगोलिक संकेतकों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत की कई पारंपरिक वस्तुएँ,जैसे दार्जिलिंग चाय,बनारसी साड़ी,नागपुरी संतरा और अन्य उत्पाद,विश्व स्तर पर अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। इन भौगोलिक संकेतकों का मजबूत संरक्षण भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ प्रीमियम मूल्य दिलाने में सहायक होगा।
पैनल ने सीईटीए से जुड़ी कई भ्रांतियों का भी समाधान किया। उन्होंने कहा कि अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते भारत की नीतिगत संभावनाओं को सीमित कर देते हैं,लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। यह समझौता भारत को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप नियम बनाने की क्षमता को और मजबूत करता है। साथ ही यह भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अधिक भरोसेमंद और आकर्षक साझेदार के रूप में प्रस्तुत करता है।
इसके अलावा,पैनल ने यह भी कहा कि यह अध्याय भारत के मौजूदा कानूनी ढाँचे और उसकी प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। इससे वैश्विक साझेदारों और निवेशकों को यह संदेश जाएगा कि भारत एक दूरदर्शी और मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था विकसित कर रहा है। यह संकेत निवेश आकर्षित करने और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत करने में सहायक होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-यूके सीईटीए का यह अध्याय केवल कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि इसका व्यापक प्रभाव भारत के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। स्वास्थ्य,शिक्षा,कृषि, उद्योग और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत वैश्विक स्तर पर अपने नवाचार और उत्पादकता को नए आयाम दे सकेगा।
इस सेमिनार ने यह संदेश दिया कि भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते में शामिल आईपीआर प्रावधान केवल कानूनी औपचारिकता नहीं हैं,बल्कि वे भारत की विकास यात्रा को गति देने और जनहित की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का माध्यम भी हैं। नवाचार और पहुँच के बीच संतुलन बनाने का यह प्रयास भारत के स्टार्टअप्स,एमएसएमई,पारंपरिक उत्पादकों और समूचे समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ ही यह भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश में एक मजबूत और विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करेगा,जो आने वाले समय में देश के आर्थिक और तकनीकी विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।